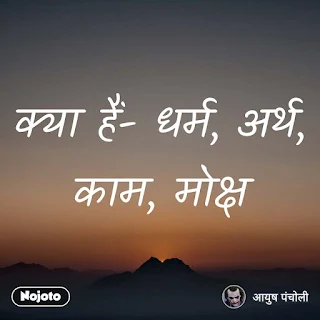मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ये 4 हैं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। लेकिन इन चारों का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, अर्थ नहीं। धर्म के अनुकूल आचरण करो तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। अर्थ से धर्म कमाना है, धर्म से अर्थ नहीं कमाना। धन केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत कमाओ।
पुरुषार्थ दो शब्दों से बना है- पुरुष तथा अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का मतलब है लक्ष्य। इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन। इसके लिए वह जिन उपायों को अपनाता है वे ही पुरुषार्थ हैं। हिंदू चिंतन के अनुसार इस पुरुषार्थ के चार अंग हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे महान ऋषियों ने मानव जीवन में इन अंगों को अनिवार्य मानते हुए इन्हें अपनाने का उपदेश दिया है।
अच्छे कपड़े हों, महंगे आभूषण हों, दुनिया भर के संसाधन हों, इन सबकी जीवन के लिए जरूरत है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि केवल इन्हीं में उलझे रहें।
सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अर्थ नहीं कमाना है। हम दान कर सकें, इसलिए भी धन कमाना है। हम परमार्थ में उसको लगा सकें इसलिए भी कमाना है। वर्ना अर्थ, अनर्थ का कारण बनेगा। धन परमार्थ की ओर भी ले जाएगा और इससे अनर्थ भी हो सकता है इसीलिए धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं और अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु इस जीवन को चलायमान रखना है। केवल इंद्रियों को तृप्त करना काम का उद्देश्य नहीं है।
काम इसलिए है कि जीवन चलता रहे। मकान, कपड़ा, रोटी ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसी तरह जीवन की आवश्यकता है काम ताकि जीवन चलता रहे, वंश परम्परा चलती रहे।
धर्म क्या है?
पुरुषार्थों में पहला स्थान धर्म का है। जीवन में जो भी धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। धर्म मनुष्य को अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। 'महाभारत' के अनुसार धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता। धर्म में लोककल्याण की भावना निहित है। मनु के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है, धर्म उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति इस संसार में तथा परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य समाज में रहकर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है। धर्म उसके सामाजिक आचरण को एक निश्चित और सकारात्मक रूप देता है।
भारतीय संस्कृति में अर्थ का क्या महत्व है?
अर्थ का सीधा संबंध जीवनयापन करने में सहायक भौतिक उपादानों से है।
अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय संस्कृति में परलोक एवं मोक्ष को ही प्रमुखता दी गई है, इहलोक (सांसारिक जीवन) वहां उपेक्षित है। यह एक गलत धारणा है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में इहलोक एवं परलोक दोनों को समान महत्व दिया गया है। मनुष्य के इहलौकिक एवं पारलौकिक उद्देश्यों के मध्य जितना उदात्त एवं उत्कृष्ट सामंजस्य भारतीय संस्कृति में है उतना किसी अन्य संस्कृति में नहीं। इसी सामंजस्य के कारण ही भारत जहां दर्शन के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचा, वहीं उसकी भौतिक उपलब्धियां भी विशिष्ट रहीं।
यह सही है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, किंतु अर्थ का महत्व भी इस संस्कृति में कम नहीं है। अर्थ को यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता तो भारत संभवत: अर्थ का दास बनकर ही रह जाता।
काम का मर्यादित रूप क्या है?
भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों के अंतर्गत काम की भी गणना की गई है। मनुष्य के जीवन में काम का भी उतना ही महत्व है, जितना धर्म व अर्थ का। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति का नाम है- काम। आहार, निदा, भय एवं काम मनुष्य एवं पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मगर मनुष्य एक सामाजिक एवं बुद्धिसंपन्न प्राणी है। वह प्रत्येक कार्य बुद्धि की सहायता से करता है। पशुओं में काम स्वाभाविक रूप से होता है। उनमें विचार तथा भावना नहीं होती है। मनुष्य का काम संबंध शिष्ट एवं नियंत्रित होता है। मनुष्य के इस व्यवहार को मर्यादित करने के लिए स्त्री-पुरुष संबंध को स्थायी, सभ्य एवं सुसंस्कृत रूप दिया गया। विवाह द्वारा मनुष्य की उच्छृंखल काम वासना को मर्यादित किया गया। भारतीय परंपरा में काम का उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है, काम वासना की पूर्ति नहीं।
मोक्ष कैसे संभव है?
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थों में गहरा संबंध है। मोक्ष से धर्म का प्रत्यक्ष संबंध है। सभी प्राणी केवल धर्म का आश्रय ग्रहण कर तथा उसी के अनुसार आचरण कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अर्थ एवं काम का सेवन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे। कौटिल्य ने कहा है कि व्यक्ति संसार में रहकर सारे ऐश्वर्य प्राप्त करे, उपभोग करे, धन संचय करे, किंतु सब धर्मानुकूल हो। उनके मूल में धर्म का अनुष्ठान हो। काम के लिए भी वात्स्यायन ने कामसूत्र में कहा है कि वही काम प्रवृत्ति पुरुषार्थ के अंतर्गत आ सकती है जो धर्म के अनुरूप हो। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि धर्मपूर्ण काम में ईश्वर विद्यमान रहता है। इस प्रकार धर्मानुकूल अर्थ व काम का सेवन करने से मनुष्य परम पुरुषार्थ- मोक्ष के समीप पहुंचता है।
पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करती है। पुरुषार्थों के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हो पाता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है।
यह सही है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, किंतु अर्थ का महत्व भी इस संस्कृति में कम नहीं है। अर्थ को यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता तो भारत संभवत: अर्थ का दास बनकर ही रह जाता।
काम का मर्यादित रूप क्या है?
भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों के अंतर्गत काम की भी गणना की गई है। मनुष्य के जीवन में काम का भी उतना ही महत्व है, जितना धर्म व अर्थ का। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति का नाम है- काम। आहार, निदा, भय एवं काम मनुष्य एवं पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मगर मनुष्य एक सामाजिक एवं बुद्धिसंपन्न प्राणी है। वह प्रत्येक कार्य बुद्धि की सहायता से करता है। पशुओं में काम स्वाभाविक रूप से होता है। उनमें विचार तथा भावना नहीं होती है। मनुष्य का काम संबंध शिष्ट एवं नियंत्रित होता है। मनुष्य के इस व्यवहार को मर्यादित करने के लिए स्त्री-पुरुष संबंध को स्थायी, सभ्य एवं सुसंस्कृत रूप दिया गया। विवाह द्वारा मनुष्य की उच्छृंखल काम वासना को मर्यादित किया गया। भारतीय परंपरा में काम का उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है, काम वासना की पूर्ति नहीं।
मोक्ष कैसे संभव है?
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थों में गहरा संबंध है। मोक्ष से धर्म का प्रत्यक्ष संबंध है। सभी प्राणी केवल धर्म का आश्रय ग्रहण कर तथा उसी के अनुसार आचरण कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अर्थ एवं काम का सेवन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे। कौटिल्य ने कहा है कि व्यक्ति संसार में रहकर सारे ऐश्वर्य प्राप्त करे, उपभोग करे, धन संचय करे, किंतु सब धर्मानुकूल हो। उनके मूल में धर्म का अनुष्ठान हो। काम के लिए भी वात्स्यायन ने कामसूत्र में कहा है कि वही काम प्रवृत्ति पुरुषार्थ के अंतर्गत आ सकती है जो धर्म के अनुरूप हो। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि धर्मपूर्ण काम में ईश्वर विद्यमान रहता है। इस प्रकार धर्मानुकूल अर्थ व काम का सेवन करने से मनुष्य परम पुरुषार्थ- मोक्ष के समीप पहुंचता है।
पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करती है। पुरुषार्थों के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हो पाता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है।
- हर घड़ी ख़ुद से उलझना है मुक़द्दर मेरा-
- विशिष्ट कवियों की चयनित कविताओं की सूची (लिंक्स)
- स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से -गोपालदास "नीरज"
- यात्रा और यात्री - हरिवंशराय बच्चन
- शक्ति और क्षमा - रामधारी सिंह "दिनकर"
- राणा प्रताप की तलवार -श्याम नारायण पाण्डेय
- वीरों का कैसा हो वसंत - सुभद्राकुमारी चौहान
- सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोसिताँ हमारा-अल्लामा इकबाल
- कुछ बातें अधूरी हैं, कहना भी ज़रूरी है-- राहुल प्रसाद (महुलिया पलामू)
- पथहारा वक्तव्य - अशोक वाजपेयी
- कितने दिन और बचे हैं? - अशोक वाजपेयी
- उन्हें मनाने दो दीवाली-- डॉ॰दयाराम आलोक
- राधे राधे श्याम मिला दे -भजन
- ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का
- हम आपके हैं कौन - बाबुल जो तुमने सिखाया-Ravindra Jain
- नदिया के पार - जब तक पूरे न हो फेरे सात-Ravidra jain
- जब तक धरती पर अंधकार - डॉ॰दयाराम आलोक
- जब दीप जले आना जब शाम ढले आना - रविन्द्र जैन
- अँखियों के झरोखों से - रविन्द्र जैन
- किसी पत्थर की मूरत से मुहब्बत का इरादा है - साहिर लुधियानवी
- सुमन कैसे सौरभीले: डॉ॰दयाराम आलोक
- वह देश कौन सा है - रामनरेश त्रिपाठी
- बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ -महादेवी वर्मा
- मधुर-मधुर मेरे दीपक जल - महादेवी वर्मा
- प्रणय-गीत- डॉ॰दयाराम आलोक
- गांधी की गीता - शैल चतुर्वेदी
- तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार -शिवमंगलसिंह सुमन
- सरहदें बुला रहीं.- डॉ॰दयाराम आलोक
- हम पंछी उन्मुक्त गगन के-शिवमंगल सिंह 'सुमन'
- जंगल गाथा -अशोक चक्रधर
- मेमने ने देखे जब गैया के आंसू - अशोक चक्रधर
- सूरदास के पद
- रात और प्रभात.-डॉ॰दयाराम आलोक
- घाघ कवि के दोहे -घाघ
- मुझको भी राधा बना ले नंदलाल - बालकवि बैरागी
- बादल राग -सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला"
- आओ आज करें अभिनंदन.- डॉ॰दयाराम आलोक
- प्रेयसी-सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
- राम की शक्ति पूजा -सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला"
- आत्मकथ्य - जयशंकर प्रसाद
- गांधी के अमृत वचन हमें अब याद नहीं - डॉ॰दयाराम आलोक
- बिहारी कवि के दोहे
- झुकी कमान -चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी'
- कबीर की साखियाँ - कबीर
- भक्ति महिमा के दोहे -कबीर दास
- गुरु-महिमा - कबीर
- तु कभी थे सूर्य - चंद्रसेन विराट
- सरहदें बुला रहीं.- डॉ॰दयाराम आलोक
- बीती विभावरी जाग री! jai shankar prasad
- हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
- मैं अमर शहीदों का चारण-श्री कृष्ण सरल
- हम पंछी उन्मुक्त गगन के -- शिवमंगल सिंह सुमन
- उन्हें मनाने दो दीवाली-- डॉ॰दयाराम आलोक
- रश्मिरथी - रामधारी सिंह दिनकर
- अरुण यह मधुमय देश हमारा -जय शंकर प्रसाद
- यह वासंती शाम -डॉ.आलोक
- तुमन मेरी चिर साधों को झंकृत और साकार किया है.- डॉ॰दयाराम आलो
- स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से ,गोपालदास "नीरज"
- सूरज पर प्रतिबंध अनेकों , कुमार विश्वास
- रहीम के दोहे -रहीम कवि
- जागो मन के सजग पथिक ओ! , फणीश्वर नाथ रेणु
- रात और प्रभात.-डॉ॰दयाराम आलोक