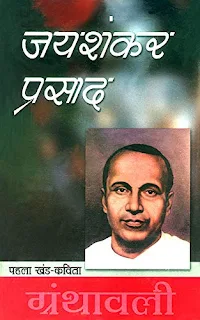शायरियो का शौक रखने वाला हर इन्सान मिर्जा ग़ालिब के नाम से वाकिफ होगा | Mirza Ghalib को शायरी शब्द का पर्यायवाची भी कह सकते है | उनके द्वारा लिखी शायरिया बच्चे जवान और बुढो सबको पसंद आती है | Mirza Ghalib की शायरिया ना केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि विश्व के कई देशो में मशहूर है | ग़ालिब ने अपने 70 साल के जीवन में कई शायरिया लिखी है | उनकी शायरियो से पहले हम उनकी जीवनी पर एक नजर डालते है |
मिर्जा ग़ालिब का प्रारम्भिक जीवन
मिर्जा ग़ालिब का जन्म आगरा के काला महल में हुई थी | Mirza Ghalib का परिवार ऐबक परिवार से सम्बन्ध रखता था जो सेल्जुक राजाओ के पतन के बाद समरकंद , अफ़ग़ानिस्तान आ गये थे | Mirza Ghalib के दादाजी मिर्जा कुकन बैग खान सेल्जुक वश के थे जो अहमद शाह के पतन के बाद समरकंद से भारत आ गये थे | उन्होंने दिल्ली ,जयपुर और आगरा काम किया और अंत में आगरा में ही बस गये | उनके चार बेटे और तीन बेटिया थी | मिर्जा अब्दुला बैग खान और मिर्जा नसरुल्ला बैग खान उनके दो बेटो के नाम थे और बाकि के बारे में ज्यादा इतिहास में जानकारी नही है |
मिर्जा अब्दुला बैग खान [मिर्जा ग़ालिब के पिताजी ] ने एक कश्मीरी लडकी इज्जत-उत-निसा बेगम से निकाह किया और वो अपने ससुराल में रहने लग गये | उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहा काम किया | उनकी 1803 में अलवर में युद्ध के दौरान मौत हो गयी और उस समय मिर्जा ग़ालिब केवल पांच साल के थे | Mirza Ghalib के चाचा मिर्जा नसरुल्ला बैग खान ने उनका पालन पोषण किया |
ग़ालिब ने 11 वर्ष की उम्र से ही शायरिया लिखना शुरू कर दिया | Mirza Ghalib सबसे पहले उर्दू में शायरिया लिखते थे हालंकि उनको पारसी और तुर्की भाषा भी आती थी | उनको स्कूल में बचपन में ही पारसी और अरबी भाषा सिखाई गयी | ग़ालिब के बचपन में एक इरानी पर्यटक ने उनको दो साल तक उनके घर रहकर पारसी और अरबी भाषा सिखाई | Mirza Ghalib की अधिकतर पुरानी गजलो में प्यार करने वालो का लिंग और पहचान का पता नही लग सकता है | उनकी प्यार पर लिखी गयी शायरिया पुरे विश्ब में मशहूर है |
केवल 13 वर्ष की उम्र में उनका निकाह नवाब इलाही बक्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया |इसके बाद वो अपने छोटे भाई मिर्जा युसूफ खान के साथ दिल्ली में बस गये लेकिन उनके छोटे भाई की एक दिमागी बीमारी की वजह से चोटी उम्र में ही मौत हो गयी | उनके सात बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गये थे | उन्होंने सोचा अब ये दुःख तो जीवन के साथ ही खत्म होगा | उन्होंने एक कविता में भी इसका जिक्र किया “”क़ैद-ए-हयात-ओ-बंद-ए-ग़म, अस्ल में दोनों एक हैं,मौत से पहले आदमी ग़म से निजात पाए क्यूँ? |
1850 में बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में उनको दबीर-उल-मुल्क की उपाधि दी गयी | इसके अलावा उनको “मिर्जा नोशा” ख़िताब से भी नवाजा गया | 1854 में खुद बहादुर शाह जफर ने उनको अपना कविता शिक्षक चुना | मुगलों के पतन के दौरान उन्होंने मुगलों के साथ काफी वक़्त बिताया |मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनको कभी पुरी पेंशन भी नहीं पायी |
Mirza Ghalib ग़ालिब की मुगल दरबार में बहुत इज्जत थी और वो उन पर व्यग्य करने वालो पर शायरी लिख दिया करते थे | उनकी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में मौत हो गयी | Mirza Ghalib पुरानी दिल्ली के जिस मकान में रहते थे उसको ग़ालिब की हवेली कहा जाने लगा और बाद में उसे एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया |Mirza Ghalib ग़ालिब की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में निजामुद्दीन ओलिया के नजदीक बनाई गयी | और उनकी मजार पर लिखा हुआ है |
“मजे जहा के अपने नजर में ख़ाक नहीं ,सिवा ए खून ए जिगर सो जिगर में ख़ाक नहीं “
भारतीय सिनेमा ने Mirza Ghalib मिर्जा ग़ालिब के सम्मान में 1954 में मिर्जा ग़ालिब फिल्म बनाई जिसमे भारत भूषण ने ग़ालिब का किरदार निभाया | इस फिल्म का संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया और कविताये उनके खुद की किताबो से ली गयी | इसी तरह पाकिस्तान में भी उनके जीवन पर फिल्म बनी जिसमे सुधीर ने ग़ालिब का किरदार निभाया था | इसके बाद 1988 भारत के मशहूर गीतकार गुलजार ने दूरदर्शन पर Mirza Ghalib मिर्जा ग़ालिब टीवी सीरियल बनाया जिसमे नसीरुद्दीन शाह ने ग़ालिब का किरदार निभाया था और इस सीरियल की गजले जगजीत सिंह द्वारा गायी गयी | यह सीरियल काफी सफल रहा और Mirza Ghalib मिर्जा ग़ालिब एक प्रसिद्ध हस्ती के रूप में उभर कर आये |
मिर्जा ग़ालिब Mirza Ghalib के जीवन पर भारत और पाकिस्तान में कई जगह पर नाटक मंचित किये गये | हालंकि गजल की दुनिया में मिर्जा ग़ालिब बहुत मशहूर हो गये थे और उनकी राह पर कई भारत और पाकिस्तान के गायक भी चले जिनमे मुख्य नाम जगजीत सिंह , मेहंदी हसन , आबिदा परवीन , फरीदा खानुम , टीना सानी , आशा भोसले , बेगम अख्तर , ग़ुलाम अली और राहत फ़तेह अली खान है |
मिर्ज़ा ग़ालिब की कुछ मशहूर शायरिया -
हाथो की लकीरों में मत जा ए ग़ालिब
किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते
किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते
हर एक बात पर कहते हो के तुम के तू क्या है
तुम्ही कहो के ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है
जिक्र उस परी वश का और फिर बयाँ अपना
बन गया रकीब आखिर था राजदान अपना
पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर ए ग़ालिब ,
या वो जगह बता जहा खुदा नहीं
कल भी कल की बात हुई आज भी कल में बीत गया ,
कल फिर कल में आज हुआ फिर यु ही जमाना बीत गया
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल ,
जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है
उन्हें देखकर चेहरे पर आती है रौनक ,
और वो समझते है बीमार का हाल अच्छा है
मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे ,
तू देख की क्या रंग है तेरा मेरे आगे
मोहब्बत में नहीं है ,फर्क जीने और मरने का ,
उसी को देखकर जीते है जिस काफिर पर दम निकले
कहू किसे मै कि क्या है शब ए ग़म बुरी बला है ,
मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता
इश्क है अपने उसूलो पे अजाल से कायम ,
इम्तेहा जिसकी भी लेता है रियायत नहीं करता
घर हमारा ,जो ना रोते तो भी , वीरान होता ,
बेहर अगर बेहर ना होता तो बयाबान होता
सैर कर दुनिया की ग़ालिब ,जिन्दगिया फिर कहा
जिंदगानी गर रही तो , नौजवानिया फिर कहा’
जलता है जिस्म जहा दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो अब राख , जुस्तजू क्या है
मस्जिद खुदा का घर है ,पीने की जगह नहीं
काफिर के दिल में जा , वहा खुदा नहीं
तेरी वफा से क्या हो , तलफी की दहर में
तेरे सिवा भी हम पर बहुत से सितम हुए
मैंने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला
होश तब आया जब उसने कहा कि, खुदा किसी एक का नहीं होता
इस कदर तोडा है मुझे उसकी बेवफाई ने ए ग़ालिब
अब कोई अगर प्यार से भी देखे तो बिखर जाता हु
कल तक तो कहते थे ग़ालिब , बिस्तर से उठा नहीं जाता
आज दुनिया से जाने की ताकत कहा से आ गयी
हजारो ख्वाहिशे ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले
बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले
दिया है दिल अगर उसको , बशर ए क्या कहिये
हुआ रकीब नामाबार है , क्या कहिये
काफिर के दिल से आया हु मै ये देखकर
खुदा मौजूद है वहा , पर उसे पता नहीं
बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना
आदमी को भी मंजूर नही इन्सान होना
कितना खौफ होता है शाम के अंधेरो में
पूंछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते
आइना देख अपना सा मुह लेके रह गये
साहब को दिल ना देने पर इतना गुरुर था
हम तो फना हो गये उसकी आँखे देखकर ग़ालिब
ना जाने वो आइना कैसे देखते होंगे |
कल तक जो जो लोग डरते थे पानी की एक बूंद से
दरिया का रुख बदलते ही तैराक बन गये
कुछ से क्या होगा , बहुत कुछ से बहुत कुछ होगा
अगर हम से ही शुरवात करे तो आगे चलकर बहुत कुछ होगा
आज क्यों लौट गया मेरा खाली घर देखकर
शायद उसे भी यकीन हुआ मेरी मोहब्बत पर
इश्क ने ग़ालिब निकम्मा बना दिया
वरना आदमे हम भी थे काम के
तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के दिखा
नहीं तो दो घूँट पी और मस्जिद को हिलता देख
इश्क पर जोर नही , है ये वो आतिश ग़ालिब
के लगाये ना लगे , बुझाये ना बुझे
लिख देना ये मिसरा मेरी संग-ए-लेहाद पर
की मौत अच्छी है मगर दिल का लगाना अच्छा नहीं
क्या सुनाऊ मै अपनी वफा की कहानी ग़ालिब
एक समन्दर का रखवाला था और सारी उम्र प्यासा रहा
ठिकाना कबर है तेरा , इबादत तू कुछ कर ग़ालिब
कहावत है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते
अक्ल वालो के मुक्कदर में ये जूनून कहा ग़ालिब
ये इश्क वाले है जो हर चीज लुटा देते है
सेहरा को बड़ा नाज है अपनी वीरानी पर
उसने देखा नही आलम मेरी तन्हाई का
ख़ाक मुट्ठी में लिए कबर की ये सोचता हु ग़ालिब
इन्सान जो मरते है तो गुरुर कहा जाता है
ज़माना रोयेगा , बरसों हमे भी याद करके
गिनेंगे सब हमारी खूबिया , जब हम ना होंगे
मै तो सुखा हुआ पत्ता हु मेरी बात ही क्या
फूल पैरो से मसलते है तेरे शहर के लोग
ज़िंदगी को गम-ए-दास्ताँ मत बना ए ग़ालिब
मुर्दा तो वो भी है जिनकी , नब्ज है धडकनों से रुक्सत
तुम्ही कहो के ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है
जिक्र उस परी वश का और फिर बयाँ अपना
बन गया रकीब आखिर था राजदान अपना
पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर ए ग़ालिब ,
या वो जगह बता जहा खुदा नहीं
कल भी कल की बात हुई आज भी कल में बीत गया ,
कल फिर कल में आज हुआ फिर यु ही जमाना बीत गया
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल ,
जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है
उन्हें देखकर चेहरे पर आती है रौनक ,
और वो समझते है बीमार का हाल अच्छा है
मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे ,
तू देख की क्या रंग है तेरा मेरे आगे
मोहब्बत में नहीं है ,फर्क जीने और मरने का ,
उसी को देखकर जीते है जिस काफिर पर दम निकले
कहू किसे मै कि क्या है शब ए ग़म बुरी बला है ,
मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता
इश्क है अपने उसूलो पे अजाल से कायम ,
इम्तेहा जिसकी भी लेता है रियायत नहीं करता
घर हमारा ,जो ना रोते तो भी , वीरान होता ,
बेहर अगर बेहर ना होता तो बयाबान होता
सैर कर दुनिया की ग़ालिब ,जिन्दगिया फिर कहा
जिंदगानी गर रही तो , नौजवानिया फिर कहा’
जलता है जिस्म जहा दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो अब राख , जुस्तजू क्या है
मस्जिद खुदा का घर है ,पीने की जगह नहीं
काफिर के दिल में जा , वहा खुदा नहीं
तेरी वफा से क्या हो , तलफी की दहर में
तेरे सिवा भी हम पर बहुत से सितम हुए
मैंने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला
होश तब आया जब उसने कहा कि, खुदा किसी एक का नहीं होता
इस कदर तोडा है मुझे उसकी बेवफाई ने ए ग़ालिब
अब कोई अगर प्यार से भी देखे तो बिखर जाता हु
कल तक तो कहते थे ग़ालिब , बिस्तर से उठा नहीं जाता
आज दुनिया से जाने की ताकत कहा से आ गयी
हजारो ख्वाहिशे ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले
बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले
दिया है दिल अगर उसको , बशर ए क्या कहिये
हुआ रकीब नामाबार है , क्या कहिये
काफिर के दिल से आया हु मै ये देखकर
खुदा मौजूद है वहा , पर उसे पता नहीं
बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना
आदमी को भी मंजूर नही इन्सान होना
कितना खौफ होता है शाम के अंधेरो में
पूंछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते
आइना देख अपना सा मुह लेके रह गये
साहब को दिल ना देने पर इतना गुरुर था
हम तो फना हो गये उसकी आँखे देखकर ग़ालिब
ना जाने वो आइना कैसे देखते होंगे |
कल तक जो जो लोग डरते थे पानी की एक बूंद से
दरिया का रुख बदलते ही तैराक बन गये
कुछ से क्या होगा , बहुत कुछ से बहुत कुछ होगा
अगर हम से ही शुरवात करे तो आगे चलकर बहुत कुछ होगा
आज क्यों लौट गया मेरा खाली घर देखकर
शायद उसे भी यकीन हुआ मेरी मोहब्बत पर
इश्क ने ग़ालिब निकम्मा बना दिया
वरना आदमे हम भी थे काम के
तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के दिखा
नहीं तो दो घूँट पी और मस्जिद को हिलता देख
इश्क पर जोर नही , है ये वो आतिश ग़ालिब
के लगाये ना लगे , बुझाये ना बुझे
लिख देना ये मिसरा मेरी संग-ए-लेहाद पर
की मौत अच्छी है मगर दिल का लगाना अच्छा नहीं
क्या सुनाऊ मै अपनी वफा की कहानी ग़ालिब
एक समन्दर का रखवाला था और सारी उम्र प्यासा रहा
ठिकाना कबर है तेरा , इबादत तू कुछ कर ग़ालिब
कहावत है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते
अक्ल वालो के मुक्कदर में ये जूनून कहा ग़ालिब
ये इश्क वाले है जो हर चीज लुटा देते है
सेहरा को बड़ा नाज है अपनी वीरानी पर
उसने देखा नही आलम मेरी तन्हाई का
ख़ाक मुट्ठी में लिए कबर की ये सोचता हु ग़ालिब
इन्सान जो मरते है तो गुरुर कहा जाता है
ज़माना रोयेगा , बरसों हमे भी याद करके
गिनेंगे सब हमारी खूबिया , जब हम ना होंगे
मै तो सुखा हुआ पत्ता हु मेरी बात ही क्या
फूल पैरो से मसलते है तेरे शहर के लोग
ज़िंदगी को गम-ए-दास्ताँ मत बना ए ग़ालिब
मुर्दा तो वो भी है जिनकी , नब्ज है धडकनों से रुक्सत
- पाटीदार जाति की जानकारी
साहित्यमनीषी डॉ.दयाराम आलोक से इंटरव्यू
गायत्री शक्तिपीठ शामगढ़ मे बालकों को पुरुष्कार वितरण
कुलदेवी का महत्व और जानकारी
ढोली(दमामी,नगारची ,बारेठ)) जाती का इतिहास
रजक (धोबी) जाती का इतिहास
जाट जाति की जानकारी और इतिहास
किडनी फेल (गुर्दे खराब ) की रामबाण औषधि
किडनी फेल रोगी का डाईट चार्ट और इलाज
प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से पेशाब रुकावट की कारगर हर्बल औषधि
सिर्फ आपरेशन नहीं ,किडनी की पथरी की १००% सफल हर्बल औषधि
सायटिका रोग की रामबाण हर्बल औषधि
बांछड़ा जाती की जानकारी
नट जाति की जानकारी
बेड़िया जाति की जानकारी
सांसी जाती का इतिहास
हिन्दू मंदिरों और मुक्ति धाम को सीमेंट बैंच दान का सिलसिला
जांगड़ा पोरवाल समाज की गोत्र और भेरुजी के स्थल
रैबारी समाज का इतिहास ,गोत्र एवं कुलदेवियां
कायस्थ समाज की कुलदेवियाँ
सुनार,स्वर्णकार समाज की गोत्र और कुलदेवी
जैन समाज की कुलदेवियों की जानकारी
चारण जाति की जानकारी और इतिहास
डॉ.दयाराम आलोक का जीवन परिचय
मीणा जाति समाज की जानकारी और गौत्रानुसार कुलदेवी
अलंकार परिचय
हिन्दी व्याकरण , विलोम शब्द (विपरीतार्थक शब्द)
रस के प्रकार और उदाहरण