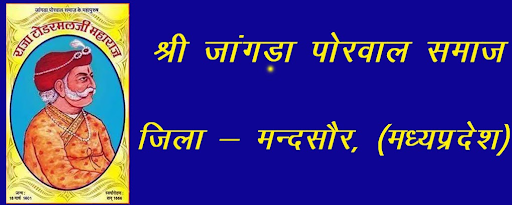भगवान श्री रजनीश साधारणतः ओशो आचार्य रजनीश और रजनीश के नाम से भी जाने जाते है, वे एक भारतीय तांत्रिक और रजनीश अभियान के नेता थे। अपने जीवनकाल में उन्हें एक विवादास्पद रहस्यवादी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था। 1960 में उन्होंने सार्वजनिक वक्ता के रूप में पुरे भारत का भ्रमण किया था और महात्मा गाँधी और हिन्दू धर्म ओथडोक्सी के वे मुखर आलोचक भी थे। मानवी कामुकता पर भी वे सार्वजनिक जगहों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, इसीलिए अक्सर उन्हें “सेक्स गुरु” भी कहा जाता था, भारत में उनकी यह छवि काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेस में लोगो ने उनके इस स्वभाव को अपनाया और उनका सम्मान किया।
आरंभिक जीवन :
एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता को उनके ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक सात वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो वो उसकी जन्म कुंडली बनायेंगे क्योंकि उनके अनुसार ओशो साथ वर्ष से अधिक जीवित नही रह सकते थे और यदि जीवित रहते है तो हर साथ वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा | इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते रहते थे | इसी कारण जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब वो एक मन्दिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे | सात दिनों तक एक वक़्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया लेकिन उनका बाल भी बांका नही हुआ था |
1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो को मौलश्री वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ | उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली | उसके बाद वो रामपुर संस्कृत कॉलेज और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे | इसी दौरान उन्होंने पुरे देश का भ्रमण किया और गांधी व् समाजवाद पर भाषण दिया | 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ | दो वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए | ओशो ने हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख , इसाई , सूफी , जैन जैसे कई धर्मो पर प्रवचन दिया था और वो अक्सर येशु ,मीरा नानक , कबीर ,गौतम बुद्ध ,दादू ,रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे |
1970 में रजनीश ने ज्यादातर समय बॉम्बे में अपने शुरुवाती अनुयायीओ के साथ व्यतीत किया था, जो “नव-सन्यासी” के नाम से जाते थे। इस समय में वे ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान ही देते थे और दुनियाभर के लोग उन्हें रहस्यवादी, दर्शनशास्त्री, धार्मिक गुरु और ऐसे बहुत से नामो से बुलाते थे। 1974 में रजनीश पुणे में स्थापित हुए, जहाँ उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहाँ भारतीय और विदेशी दोनों अनुयायीओ को “परिवर्तनकारी उपकरण” प्रदान कर सके। 1970 के अंत में मोरारी देसाई की जनता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रूकावट बना।1981 में वे अमेरिका में अपने कार्यो और गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ऑरेगोन के वास्को काउंटी के रजनीशपुरम में अपनी गतिविधियों को करने लगे।
अध्यात्मिक जीवन :
वे 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के लेक्चरर बने और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। अपने शिक्षक होने के साथ-साथ वे पुरे भारत के राज्यों में “आचार्य रजनीश” के रूप में जाकर अपने अध्यात्मिक भाषण दिया करते थे। उन्होंने समाजवाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद, विज्ञानं, प्रोद्योगिकी और जन्म नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में कई प्रकार के मुद्दों को उठाया जैसे उन्होंने रुढ़िवादी भारतीय धर्म और अनुष्ठानों की आलोचना की और कहा सेक्स(Osho Quote on Sex) अध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है।
इस भाषण के कारन उनकी बहुत आलोचना हुई पर इसकी वजह से उन्होंने और भी लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित किया। उसके बाद आमिर व्यक्ति उनसे अध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए आने लगे और उन्होंने बहुत दान भी किया और साथ ही उनके इस कार्य में भी वृद्धि हुई। 1962 में वे 3-10 दिन के ध्यान शिविर(Osho Meditation) करने लगे और जल्द ही ध्यान केन्द्रित करना उनकी शिक्षाओं में जाना-जाने लगा।
अगर हम खुले मन से सोचें तो वे एनी अध्यात्मिक नेताओं पूरी तरीके से अलग थे। 1960 के दशकों तक वे एक प्रमुख अध्यात्मिक गुरु बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षण नौकरी को छोड़ कर खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1970 में उन्हें हिन्दू नेताओं नेंकंद के तहत भारतीय प्रेस द्वारा “सेक्स गुरु” का नाम करार दिया।
जून 1964 में रणकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया और किताब में भी छापा गया। इसके बाद ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखीं, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनियाभर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, और साहित्यकारों को प्रभावित किया। 1969 में ओशो के अनुयायियो ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वह स्थान “ओशो इंटरनेशनल मैडिटेशन रिसोर्ट ” के नाम से जाना जाता है। 1980 में ओशो “अमेरिका” चले गए और वहां सन्यासियों ने “रजनीशपुरम” की स्थापना की।
ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। सन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत की विश्व को अनुपम देन बताते हुए सन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक सन्यास को पुनरुज्जीवित किया है। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती दी है। सन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज ओशो के संस्पर्श से हुआ है। इसलिए यह नव-संन्यास है। उनकी नजर में संन्यासी वह है जो अपने घर-संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में एक संन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है।
ओशो ने हजारों प्रवचन दिये। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है, आडियो कैसेट तथा विडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। अपने क्रान्तिकारी विचारों से उन्होने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाये। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब ६०० पुस्तकें हैं। संभोग से समाधि की ओर इनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इनके नाम से कई आश्रम चल रहे है। अमेरिका के लोगों की तो उनके प्रति अटूट भक्ति-भावना थी । सन् 1966 से सन् 197० तक रजनीश के अनुयायी उन्हें आचार्य कहते थे, परंतु सन् 1970 के बाद वे भगवान रजनीश हो गए । नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई । उन्होंने अपनी सफाई में कहा-‘भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है, प्रत्येक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है, जो उरानंद की अवस्था में पहुंच चुका है ।’
विचार :
• अगर आप सत्य देखना चाहते हैं तो न सहमती में राय रखिये और न असहमति में.
• केवल वह लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं वह प्रेम कर सकते हैं.
• जेन लोग बुद्ध से इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं. यह अथाह प्रेम कि वजह से है, उनमे डर नहीं है.
• किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है. आप स्वयं में जैसे भी हैं एकदम सही हैं. खुद को स्वीकार करिए.
• सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है बल्कि इसके उलट, सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है.
• दोस्ती शुद्ध प्रेम है. यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहाँ कुछ भी नहीं माँगा जाता, कोई भी शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है.
• प्रसन्नता सदभाव की छाया है, वो सदभाव का पीछा करती है. प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है.
• जीवन कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक हास्य है. जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना.
• अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं. ध्यान दर्पण में देखने की कला है.
• आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सबकुछ है, यही बिलकुल सही है, बस यही है. आत्मज्ञान यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है.
• जेन एकमात्र वह धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखाता है. इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है.
• आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं- इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जायेंगे, और कहेंगे, “अब मेरे पास प्रेम नहीं है”. जहाँ तक प्रेम का सवाल है आप दिवालिया नहीं हो सकते
म्रुत्यू :
आचार्य रजनीश ने मुंबई और पूना में अपने आश्रम बनवाए । उन्होंने 1981 में अपने शिष्यों सहित अमेरिका जाकर रजनी-पुरम की स्थापना की, लेकिन अमेरिका सरकार ने उनके कुछेक शिष्यों को गैर-कानूनी कार्यों के कारण उन्हें वहां से जाने पर विवश कर दिया । उसके बाद आचार्य रजनीश भारत लौट उगए और फिर यही उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी । 19 जनवरी 1990 को उगचार्य रजनीश ने अंतिम समाधि ले ली । उनके अनुयायियों को इस समाचार से काफी दुख हुउग । ओशो तो चले गए, परंतु उनके द्वारा दिए ज्ञान की राह पर चलकर उगज भी मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है ।
विकिपेडिया अनुसार-
ओशो (मूल नाम रजनीश) (जन्मतः चंद्र मोहन जैन, ११ दिसम्बर १९३१ - १९ जनवरी १९९०), जिन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश,या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता-नेता थे। अपने संपूर्ण जीवनकाल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। १९६० के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद, महात्मा गाँधी, और हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे, हालाँकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया।
चन्द्र मोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुच्वाडा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई धारणायें हैं। एक मान्यता के अनुसार, खुद ओशो कहते है कि ओशो शब्द कवि विलयम जेम्स की एक कविता 'ओशनिक एक्सपीरियंस' के शब्द 'ओशनिक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सागर में विलीन हो जाना। शब्द 'ओशनिक' अनुभव का वर्णन करता है, वे कहते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या? इसके लिए हम 'ओशो' शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात, ओशो मतलब- 'सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला'। १९६० के दशक में वे 'आचार्य रजनीश' के नाम से एवं १९७० -८० के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और १९८९ के समय से ओशो के नाम से जाने गये। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होने प्रवचन दिये।
रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुम्बई में शुरू किया, जिसके बाद, उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार के उपचारविधान पेश किये जाते थे. तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को ऑरगन, अमरीका में स्थानांतरण कर लिया। १९८५ में एक खाद्य सम्बंधित दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और २१ अन्य देशों से ठुकराया जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताये।
उनकी मृत्यु के बाद, उनके आश्रम, ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रेसॉर्ट को जूरिक आधारित ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन चलाती है, जिसकी लोकप्रियता उनके निधन के बाद से अधिक बढ़ गयी है।
चन्द्र मोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुच्वाडा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई धारणायें हैं। एक मान्यता के अनुसार, खुद ओशो कहते है कि ओशो शब्द कवि विलयम जेम्स की एक कविता 'ओशनिक एक्सपीरियंस' के शब्द 'ओशनिक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सागर में विलीन हो जाना। शब्द 'ओशनिक' अनुभव का वर्णन करता है, वे कहते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या? इसके लिए हम 'ओशो' शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात, ओशो मतलब- 'सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला'। १९६० के दशक में वे 'आचार्य रजनीश' के नाम से एवं १९७० -८० के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और १९८९ के समय से ओशो के नाम से जाने गये। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होने प्रवचन दिये।
रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुम्बई में शुरू किया, जिसके बाद, उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार के उपचारविधान पेश किये जाते थे. तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को ऑरगन, अमरीका में स्थानांतरण कर लिया। १९८५ में एक खाद्य सम्बंधित दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और २१ अन्य देशों से ठुकराया जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताये।
उनकी मृत्यु के बाद, उनके आश्रम, ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रेसॉर्ट को जूरिक आधारित ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन चलाती है, जिसकी लोकप्रियता उनके निधन के बाद से अधिक बढ़ गयी है।
******************
हिन्दू मंदिरों और मुक्ति धाम को सीमेंट बैंच दान का सिलसिला
दामोदर चिकित्सालय शामगढ़ के आशु लाभकारी उत्पाद
प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से पेशाब रुकावट की कारगर हर्बल औषधि
सेक्स का महारथी बनाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खे
आर्थराइटिस(संधिवात),गठियावात ,सायटिका की तुरंत असर हर्बल औषधि
सिर्फ आपरेशन नहीं ,किडनी की पथरी की १००% सफल हर्बल औषधि
तिल्ली बढ़ जाने के आयुर्वेदिक नुस्खे


.jpg)